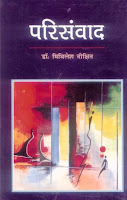‘दोहा’ हिन्दी साहित्य का महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त सशक्त छंद है और सबसे अधिक विचित्र बात यह है कि दो पंक्तियों में पूरी बात कहने, प्रकट करने की क्षमता इस छंद में है। जिस प्रकार ग़ज़ल के एक शेर में पूरी बात कही जा सकती है, उसी प्रकार दोहे की दो पंक्तियों में गागर में सागर भरा जा सकता है और यह काम हिन्दी के साहित्यकारों यथा तुलसी, कबीर, रहीम, बिहारी आदि ने बखूबी किया है। कबीर और रहीम ने तो नीतिगत सिद्धान्तों का प्रतिपादन, वर्णन बखूबी दोहों के माध्यम से किया है। कबीर की उलटवाँसियाँ समझने में नानी याद आती है।
दोहे के साथ दुम लगाने का चलन अधिक प्रचलित नहीं है किन्तु दोहे के कथ्य को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए दुम का प्रयोग जरूरी हो न हो, प्रभावी और सार्थक लगता है।
श्री शिवानन्द सिंह ‘सहयोगी’ जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इनके गीत और ग़ज़ल की अनेक पुस्तकों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला है। इनकी ग़ज़लें जितनी सहज, सरल हैं, गीत उतने ही प्रभावी और संवेदनाओं से ओत-प्रोत हैं। सहयोगी जी के दुमदार दोहे भाव, भाषा और अभिव्यक्ति में जितने सशक्त हैं, उतने ही प्रभावशाली और एक चिरस्थायी छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं।
सहयोगी जी की सद्य प्रकाशित पुस्तक ‘दुमदार दोहे’ से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं।
जहाँ बसी संवेदना, वहीं बसा है भाव
कागज पर तैरा गई, वह शब्दों की नाव
पीर का पाल सजाए।
दर्द पिघल आँसू बने, बहता है दरियाव
कविता विरही तैरती, बन अक्षर की नाव
भाव पतवार बने हैं।
बूँद-बूँद बन टपकता, अंतस का अहसास
मोती बन बन विहँसता, ठिगना सा विश्वास
भाव पर पीड़ा भारी।
कविता के बारे में जो एक प्रसिद्ध उक्ति है कि ‘वियोगी होगा पहला कवि, ......।’ सहयोगी जी के ये दोहे उसी चिरंतन सत्य को प्रतिष्ठापित करते हैं। सहयोगी जी के दोहों में मौसम अठखेलियाँ करता है और जीने का एक उत्साह, उमंग, जोश, प्रेरणा जो भी कहिए, देता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि-
धरती जब करती रहे, सुबह शाम तक काम
सूरज को मिलता प्रिये, तब कैसे विश्राम
प्रेम का ऐसा बंधन।
गुपचुप गुपचुप गगन में, रही सँवरती रात
जुगनू की डोली सजी, तारे चले बरात
चाँद का पता नहीं है।
सूरज चलता तानकर, सिर पर स्वर्णिम छाँह
छाया चलती टहलती, पकड़ धूप की बाँह
तिमिर है आने वाला।
सहयोगी जी के दोहे बहुआयामी हैं। पत्नी-पुराण के कुछ दोहे बहुमुखी, सार्थक और हृदयग्राही बन पड़े हैं-
पत्नी घर की लोरियाँ, पत्नी घर की गीति
पत्नी घर की दैनिकी, पत्नी घर की प्रीति
दया की आँख बिलौरी।
बड़ी कुमुदनी हँसमुखी, कलरव का अनुनाद
फूल झरे मुख से तभी, करती जब संवाद
कोकिला पास कुहुकती।
घर और मकान का अंतर सहयोगी जी के शब्दों में-
घर अब घर लगता नहीं, लगता एक मकान
जब से गायब है हुई, बच्चों की मुसकान
कि नफरत आँख तरेरे।
छल-प्रपंच ने फूँक दी, उसका इतना कान
अहं चला घर छोड़कर, रोता रहा मकान
निजी मजबूरी होगी।
चिन्ता करके मर गया, आधा हुआ शरीर
फिर भी धोखा दे गई, करतल खिंची लकीर
बैठ मत राम भरासे।
गाँव-गाँव हर रूाहर में, घूमा बहुत फकीर
फिर भी मजहब की नहीं, छोटी हुई लकीर
धर्म का पेच निराला।
दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा-
गंगा सागर से मिली, जहाँ रेत ही रेत
मिलन नहीं है देखता, पर्वत खाई खेत
मिलन है एक पहेली।
कहाँ तक कहें, सहयोगी जी ने अपनी बहुमुखी, बहुआयामी प्रतिभा दिखाते हुए, ग्रामीण परिवेश, पर्व त्यौहार, जीवन दर्शन, शिक्षा एवं संस्कार आदि विषयों पर भी बड़े सार्थक दोहे कहे हैं। मेरी ओर से बधाई व साधुवाद।
दुमदार दोहे : दुमदार दोहों का संग्रह। कवि : शिवानन्द सिंह सहयोगी। प्रकाशक : कुसुम प्रकाशन, 186, इंजीनियर्स कॉलोनी, क्वार्सी बरईपास रोड, अलीगढ़ (उ.प्र.),। पृष्ठ : 112। मूल्य : 120 रुपये ; संस्करण : 2012।
- 108/3, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ (उ.प्र.)
राजेन्द्र परदेशी
डॉ. मिथिलेश दीक्षित की हाइकु-रचनाधर्मिता
हिन्दी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठित पत्रकारिताभूषण डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव के द्वारा सम्पादित ग्रन्थ ‘डॉ. मिथिलेश दीक्षित की हाइकु-रचनाधर्मिता’ में हाइकु-काव्य की चर्चित और प्रतिष्ठित कवयित्री डॉ. मिथिलेश दीक्षित की हाइकु-लेखन की विविध भंगिमाओं पर, उनके शिल्प के विविध प्रयोगों पर तथा उनके आस्थापरक-मूल्यपरक चिन्तन से सम्बन्धित विविध आयामों पर देश के जाने-माने हाइकुकारों, निबन्धकारों, सम्पादकों और समीक्षकों के समीक्षात्मक आलेखों द्वारा प्रकाश डाला गया है। ग्रन्थ को चार खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में उनके हाइकु-लेखन के कथ्य एवं शिल्प पर डॉ. बी.के.सिंह, नरेश चन्द्र सक्सेना ‘सैनिक’, डॉ. सुधेश, डॉ. सुन्दर लाल कथूरिया, नलिनीकान्त, नीलमेन्दु सागर, डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र, उर्मिला कौल, डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव, डॉ. वेद प्रकाश अमिताभ, डॉ. बिन्दुजी महाराज ‘बिन्दु’, डॉ. रामनिवास ‘मानव’, रामनिवास पन्थी, श्रीकृष्ण कुमार त्रिवेदी आदि अनेक विद्वानों के समीक्षात्मक आलेख हैं। द्वितीय खण्ड में उनके हाइकु-संग्रहों- स्वर विविध क्षणबोध के, सदा रहे जो, तराशे पत्थरों की आँख, लहरों पर धूप, एक पल के लिए, अमरबेल आदि पर प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. भगवतशरण अग्रवाल, डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा ‘अरुण’, डॉ. सन्त लाल विश्वकर्मा, डॉ. त्रिभुवन राय, डॉ. मीता सिन्हा ‘आशा’, डॉ. बृजेश त्रिपाठी, यतीश चतुर्वेदी, निर्मल शुक्ल, हरिश्चन्द्र शाक्य, डॉ. शिवप्रसाद मिश्र, डॉ. राजेन्द्र मिलन आदि ने विवेचन-विश्लेषण और मूल्यांकन किया है। तृतीय खण्ड में डॉ. दीक्षित के सैकड़ों प्रतिनिधि हाइकु संग्रहीत किये गये हैं। साथ ही, उनके हाइकु लम्बी कविता, तांका, तांका-बन्ध, हाइकु-मुक्तक आदि नवीन-नवीन प्रयोग भी प्रस्तुत हुए हैं। ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड में डॉ. दीक्षित की हाइकु-रचनाधर्मिता पर उनके प्रकाशित हाइकु-ग्रन्थों पर देश के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 100 विद्वानों के अभिमत तथा उन पर तथा प्रकाशित हाइकु-साहित्य पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ दी गयी हैं। हिन्दी हाइकु जगत में किसी हाइकुकार की समग्र हाइकु रचनाधर्मिता पर विस्तृत कलेवर (दो सौ चौबीस पृष्ठों) का यह प्रथम ग्रन्थ है।
डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव ने स्वयं ही प्रकाश डाला है कि डॉ. मिथिलेश दीक्षित की रचनाओं में अद्भुत प्रवाहमयता, तारतम्य, गुम्फन एवं शिल्प-संयोजन है। उनके अनेक कालजयी हाइकु मराठी, बंगला और अंग्रेजी में अनूदित हो चुके हैं। अनेक अनुवाद-रूप में संकलनों में भी समाविष्ट हुए हैं। अपने देश की एक कर्मठ, जागरूक एवं तेजस्विनी सृजनकत्री डॉ. दीक्षित की हाइकु-रचनाधर्मिता का एक साथ परिचय प्राप्त हो सके, अपनी रचनाओं के माध्यम से, आस्था और प्रेम का सन्देश देने वाली, मानवतावादी कवयित्री, निबन्धकार और समीक्षक इस विदुषी के चिन्तन और हाइकु काव्य-कला की जानकारी पूरी दुनियां को मिल सके, इस प्रयोजन से पुस्तक प्रकाश में लायी जा रही है। कृतित्व से पूर्व व्यक्तित्व की एक झलक मात्र देने के कारण, पुस्तक के प्रारम्भ में दो आलेख दिये गये हैं। देश के विभिन्न राज्यों के हिन्दी रचनाकारों, शिक्षकों एवं समीक्षकों ने डॉ. मिथिलेश दीक्षित के लेखन की मुक्तकंठ से सराहना की है।
डॉ. मिथिलेश दीक्षित कर हाइकु-रचनाधर्मिता : व्यक्तित्व व कृतित्व विवेचन। सम्पादक : डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव। प्रकाशक : अमित प्रकाशक, गाजियाबाद (उ.प्र.)। मूल्य : रु.350/-। संस्करण : 2011।
- भारतीय साहित्य अकादमी, चाँदन रोड, फरीदी नगर, लखनऊ-226015 (उ.प्र.)
डॉ. उमेश महादोषी
बबूल के जंगल से गुजरती कुछ सकारात्मक कहानियाँ
हमारे देश में पौराणिक/धार्मिक महत्व के शहरों की एक खास विशेषता है, इन शहरों के भौतिक एवं चारित्रिक दृष्टि से जितना साफ-सुथरे होने की अपेक्षा/संकल्पना की जाती है, वास्तव में ये उतने ही हर प्रकार की गंदगी से भरे हुए हैं। हरि यानी ईश्वर के धामों का प्रवेश द्वार माना जाने वाला हरिद्वार शहर भी इससे अछूता नहीं है। इस धार्मिक महानगरी में यूँ तो धर्म साक्षात स्वरूप में विचरण करता-सा दिखता है, लेकिन कोई खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति थोड़ा सा भी इसके अन्दर झाँककर देखने का प्रयास करे तो भौतिक गंदगी के साथ-साथ चारित्रिक गंदगी का बहुत बड़ा साम्राज्य इस शहर के बदन पर भयंकर कोढ़-सदृश दिखाई दे जायेगा। सुप्रसिद्ध कथाकार श्री के.एल. दिवान के नये कहानी संग्रह ‘बबूल के जंगल और उम्मीद के फूल’ की कई कहानियों में इस शहर की महागन्दगी पहाड़ों पर पानी के सोतों की तरह फूट पड़ी है। दिवान साहब के जीवन का अधिकांश हिस्सा इसी शहर में बीता है। उन्होंने अपनी साहित्य साधना और शिक्षा के क्षेत्र में किया सारा का सारा अवदान इसी शहर की धरती पर बैठकर किया है। स्वाभाविक है उनके अनुभवों में इस शहर की मिट्टी के कण-कण का रूप-स्वरूप गहरे तक पैठा होगा। उन्होंने शहर की गन्दगी (जो सिर्फ इस शहर की ही नहीं है अब सर्वव्यापी हो गई है) और उसके दुष्परिणामों को देखा है। दूसरी ओर चूँकि वह उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके कुछ आदर्श थे, उसूल थे; जिनके लिए जीवन के बड़े-बड़े सुखों को कुर्बान किया जा सकता था। ऐसे में सड़ांध युक्त कीचड़ में लोटते सुअरों को और उनके साथ गाय-बैलों, हिरणों, घोड़ों आदि को भी, वह भी हरिद्वार जैसे शहर में देखते होंगे, तो दुःख तो होगा ही होगा। अपनी इस पीड़ा को उन्होंने एक साहित्यकार के रूप में सिर्फ व्यक्त ही नहीं किया है, अपितु उसके दुष्परिणामों के प्रति आगाह भी किया है और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। मार्गदर्शन इस रूप में कि ऐसी स्थितियों से जनित तमाम निराशाओं के मध्य भी एक लेखक के रूप में वह उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ते और इसकी छाप पाठक के मनोमस्तिष्क में भी सफलतापूर्वक उतारते दिखाई देते हैं।
इस कहानी संग्रह में छोटी-बड़ी बारह कहानियाँ संग्रहीत हैं। बबूल का जंगल, फिसलते-फिसलते, दरार, परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम, मौत बांटती मांगती जिन्दगियाँ, जिन्दगी के दो सिपाही कहानियों में कथाकार ने उस गन्दगी को बखूबी बेपर्दा किया है, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संकेतों को समझकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इसका प्रेरणा स्रोत हरिद्वार के वातावरण में ही निहित है। ‘बबूल का जंगल’ में उन्होंने साधु-संतों के पास जमा अकूत धन का कैसा उपयाग होता है और उससे कैसे-कैसे भक्त पैदा होते हैं, उस अकूत धन से रिश्तों और मर्यादाओं की कैसी-कैसी परिभाषाएँ लिखी जाती हैं, इसे विस्तार से दर्शाया है। यद्यपि यह कहानी भाषा के स्तर पर कुछ ढीली पड़ गयी है, तदापि नायिका को जिस प्रकार संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभारा है, उससे कहानी अन्ततः अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रही है। ‘फिसलते-फिसलते’ एवं ‘जिन्दगी के दो सिपाही’ कहानियों में अय्यासी की गन्दगी के दुष्परिणामों को तो दर्शाया ही है, समाज सेवा के बहाने ‘वैगर हाउस’ एवं नारी निकेतन बगैरह जैसे सामाजिक संस्थानों के दुरुपयोग की असलियत भी प्रभावी ढंग से सामने रखी गयी है। अय्यासी का अन्धापन किस तरह माँ समान सास और दामाद के पवित्र रिश्ते को भी तार-तार कर देता है, इसे ‘दरार’ कहानी में दर्शाया गया है। ‘फिसलते-फिसलते’ में यद्यपि दिवान साहब अपनी पीढ़ी के परम्परागत दृष्टिकोंण से आत्महत्या के विचार के ऊपर जीवन की प्रेरणा का सन्देश देने में सफल रहे हैं, परन्तु अय्यासी के लिए रिश्तों को तार-तार कर देने वालों को जाने-अनजाने खुला छोड़ गये हैं। ‘परिवर्तन की ओर बढ़ते कदम’ में तमाम गन्दगी को उघाड़ते हुए भी दिवान साहब एक बेहद सकारात्मक और चिन्तनशील दृष्टिकोंण लेकर सामने आते हैं। वह एक शिक्षाशास्त्री भी हैं और शिक्षा के प्रकाश को फैलाने के प्रबल पक्षधर भी। इस बात को उन्होंने इस कहानी, खासकर कहानी के अन्त में जो सपना-सा वह कहानी के नायक की आँखों में डालते हैं, के माध्यम से स्पष्टतः रखा है। पर एक खास बात इस कहानी में और है, तथाकथित पढ़े-लिखे, सभ्य और बड़े कहे जाने वाले लोगों में शिक्षा का प्रतिबद्धित प्रभाव देखने को नहीं मिलता, वह प्रभाव अक्सर अनपढ़, गंवार और पथभ्रष्ट कहे जाने वाले खानाबदोश बंजारों में भी दिख जाता है। कहानी के नायक और मनचली उर्फ ममता के मध्य चर्चा में ममता के मुख से निकले इन शब्दों पर गौर कीजिए- ‘......अजीब बात है हमें बुरी लड़कियाँ कहा जाता है....आपसे पढ़कर अंकल मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहती। फिर......हम अपने गुरुओं को पथभ्रष्ट नहीं करते.......मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊगी।’ निश्चित रूप से कहानी का यह प्रसंग कृत्रिम नहीं है, लेखक ने थोपा नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रसंग है। एक आस्था है, एक चिन्तन है, एक दर्शन है; अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिबद्धित प्रभाव है, जो आंशिक रूप में ही सही तथाकथित छोटे लोगों में आज भी जीवित है। कीचड़ में खिले कमल की तरह! कहानी को यह प्रसंग एक ऊँची चोटी पर ले जाकर खड़ा कर देता है।
दिवान साहब का आशावाद और तमाम निराशाओं के मध्य भी जीवन को जीने के प्रति नजरिया कितना मजबूत और सकारात्मक है, इसे देखा जा सकता है ‘मौत बांटती मांगती जिन्दगियाँ’ कहानी में। अय्यास पिता के भ्रष्ट आचरण के प्रति विद्रोह करके कहानी की नायिका शान्ति की खोज में हरिद्वार आती है, लेकिन वहाँ भी तमाम तरह की गन्दगी के बीच उसे अशान्ति ही मिलती है। लेकिन लेखक इस अशान्ति के मध्य भी बेहद स्वाभाविक ढंग से जीवन को जीने का रास्ता दिखा देता है। यह निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी से वरिष्ठ पीढ़ी के सृजक की एक अपेक्षा है, एक सम्भावना है जिसे लेखक युवा पीढ़ी में टटोलता है, यह एक लेखक की सृजनात्मकता है। यही कहानी की उद्देश्यपरकता हो सकती है।
अन्य कहानियों में ‘कपड़ा’ एक संवेदना प्रधान सकारात्मक कहानी है। इस कहानी में आजादी के बाद देश के बँटबारे के समय की भयावहता के स्मरण में कुछ सकारात्मक दृश्यों को डालकर साम्प्रदायिक सद्भाव की पक्षधरता को भी दर्शाया गया है। ‘कपड़ा’ में संवेदना के साथ सकारात्मक कल्पनाशीलता देखने को मिलती है, जो कभी-कभी यथार्थ की धरती पर भी उतरती दिखाई दे जाती है।
‘मदर्स डे’ एवं ‘मुलाकात मास्टर गुलाब सिंह से’ कहानियों में वृद्धों के प्रति सन्तानों के उपेक्षा-भाव को उजागर किया गया गया है। लेकिन ‘मदर्स डे’ में इस उपेक्षा पर जहाँ सकारात्मक संवेदना को पूरी सिद्दत से तरजीह दी गयी है, वहीं ‘मुलाकात मास्टर गुलाब सिंह से’ में वृद्धावस्था के संघर्ष को। ‘मदर्स डे’ में एक बार फिर लेखक ने युवा पीढ़ी पर अपना भरोसा जताया है और उससे अपनी अपेक्षाओं को उजागर भी किया है। अनुभवों के धनी दिवान साहब जानते हैं, मूल तो गया, ब्याज समय पर और ईमानदारी से मिलता रहे तो समय की धड़कनें अपनी गति खोने से बच जायेंगी। ‘अपनों से सच्ची मुलाकात’ में चारित्रिक गन्दगी में पैदा होते रिश्तों की सडांध के यथार्थ को दर्शाया गया है। लेकिन लेखक इस सड़ांध के यथार्थ के खिलाफ संघर्ष के बाज को अपने कंधे पर बैठाकर चलता है, जो एक झपट्टा मारता है और तथाकथित पारिवारिक मर्यादाओं के भ्रमजाल को पंजे में दबाकर उड़ जाता है। कहानी का अन्त प्रभावित करता है। बाकी बची एक कहानी ‘कड़वाहट’ में मुझे कहानी नज़र नहीं आई। इसे क्या कहूँ.....शायद यथार्थपरक कथ्य प्रधान गद्य-गीत कहने से काम चल जाये।
संग्रह का शीर्षक काफी बड़े आकार का हो गया है और ऐसा लगता है, जैसे किन्ही दो कहानियों के शीर्षकों को मिलाकर बनाया गया हो। परन्तु ऐसा है नहीं। ‘बबूल का जंगल’ शीर्षक से तो एक कहानी इस संग्रह में है, पर ‘उम्मीद के फूल’ किसी कहानी का शीर्षक नहीं है। निश्चित रूप से बबूल के जिस जंगल से होकर ये कहानियां गुजरती हैं, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोंण का एक पेड़ भी दिखाई देता है और उस पर खिले हुए लेखक की उम्मीदों के फूल भी। हो न हो शीर्षक यहीं से आया है और अपनी सार्थकता भी सिद्ध करता है। प्रूफ की कई गलतियाँ अखरती हैं, कुछ शब्द तो जब एक जगह गलत हुए तो आगे गलत होते ही गये हैं। आवरण थोड़ा आकर्षक और वाइन्डिग मजबूत होती तो पुस्तक भौतिक रूप में भी ज्यादा अच्छी लगती।
बबूल का जंगल और उम्मीद के फूल : कहानी संग्रह। कथाकार : के. एल. दिवान। प्रकाशक : हिन्दी साहित्य साधना प्रकाशन, ज्ञानोदय अकादमी, 8, निर्मला छावनी, हरिद्वार-249401 (उत्तराखंड)/मूल्य : रु. 200/- मात्र/पृष्ठ 100, संस्करण : नवम्बर 2011।
- एफ-488/2,गली सं.11,राजेन्द्रनगर, रुड़की-247667, जिला-हरिद्वार (उत्तराखंड)
यतीश चतुर्वेदी ‘राज’
हाइकु जगत का वृहद् साक्षात्कार संकलन
हिन्दी साहित्य की सुप्रसिद्ध हाइकुकार एवं समीक्षक डॉ. मिथिलेश दीक्षित के द्वारा सम्पादित ‘परिसंवाद’ हिन्दी हाइकु जगत का प्रथम वृहद् साक्षात्कार संग्रह है, जिसमें प्रसिद्ध समीक्षकों एवं हाइकुकारों के हाइकु-काव्य के विषय में डॉ. दीक्षित के द्वारा लिये गये साक्षात्कार संकलित हैं। ग्रन्थ में विभिन्न विद्वानों के साक्षात्कारों द्वारा हाइकु-कविता के उद्भव, स्वरूप, विकास, कथ्य, शिल्प, लोकप्रियता एवं सम्भावनाओं पर पर्याप्त विवेचना है। हाइकु-काव्य के विविध आयामों पर साक्षात्कारकत्री द्वारा सुश्री उर्मिला कौल, डॉ. अंजलि देवधर, डॉ. कमल किशोर गोयनका, डॉ. भगवतशरण अग्रवाल, कमलेश भट्ट ‘कमल’, डॉ. जगदीश ‘व्योम’, नलिनीकान्त, नीलमेन्दु सागर, डॉ. सुधा गुप्ता, डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव, राधेश्याम, राजेन्द्र परदेशी, डॉ. विद्या विन्दु सिंह आदि 31 हाइकुकारों एवं समीक्षकों के साक्षात्कार लिये गये हैं। उर्मिला कौल ने हाइकु को परिभाषित करते हुए कहा कि यह जीवन के साक्षात्कार का अनुभूति-प्रधान बिम्बात्मक काव्य है। डॉ. कमल किशोर गोयनका ने बताया कि हाइकु मूलतः अनुभूति की कविता है। मानव मन जब घनीभूत अनुभूतियों से आवेगमय होता है तथा उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म आवेग अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होते हैं, तो हाइकु का जन्म होता है। हाइकु का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध है, परन्तु यह ऋतुकाव्य न होकर ऋतुबोध का काव्य है। कमलेश भट्ट ‘कमल’ के अनुसार इण्टरनेट पर हाइकु ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि के साथ पहले ही अच्छा-खासा स्थान प्राप्त कर लिया है। राधेश्याम के अनुसार हाइकु का प्रत्येक शब्द एक अनुभूति का दर्पण है। हाइकु कविता शुद्ध अनुभूति के सूक्ष्म आवेगों की सरलतम एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लय, ध्वनि, शब्दार्थ ही हाइकु का सौन्दर्य है। नीलमेन्दु सागर ने हाइकु के निर्धारित शिल्प की अनिवार्यता पर बल दिया है। उनके विचार से हाइकु के लिए परम्परागत शिल्प की प्रतिबद्धता सर्वथा उपयुक्त है, अन्यथा वह हाइकु नहीं रहकर कुछ और हो जायेगा। डॉ. बिन्दुजी महाराज ‘बिन्दु’ ने ऋतुबोध को हाइकु की विशिष्ट पहचान माना है। डॉ. भगवताशरण अग्रवाल हाइकु का भविष्य सभी सन्दर्भों में उज्जवल मानते हैं। डॉ. रमाकान्त श्रीवास्तव ने हाइकु को अलंकारविहीन गहन अभिव्यक्ति की कविता माना है। राजेन्द्र परदेशी हाइकु के भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। वे मानते हैं कि हाइकु के साथ उसका युग जुड़ा है। डॉ. मिथिलेश दीक्षित ने अपने सम्पादकीय में स्पष्ट कर दिया कि लय तो हाइकु-कविता में सौन्दर्य के रंग भर देती है, तुकान्तता हो या नहीं हो। तुकबन्दी के प्रयास में कभी-कभी कविता में सम्प्रेषणीयता बाधित हो जाती है; सटीक शब्दावली का अभाव हो जाता है, प्रासंगिकता और प्रयोजन में व्यवधान आ जाता है, क्योंकि कविता में शिल्प से पहले कथ्य महत्वपूर्ण होता है। भावों के सहज प्रवाह में तुकान्तता अल्पायास ही आ जाये, तो बहुत ठीक है, अन्यथा बनावट से आकृति बनी रहती है, आत्मा विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार सृजन, शोध एवं समीक्षा के क्षेत्र में भी यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण है।
परिसंवाद : डॉ. मिथिलेश दीक्षित द्वारा हाइकु विषयक साक्षात्कारों का संग्रह। सम्पादक : डॉ. मिथिलेश दीक्षित। प्रकाशक : समन्वय प्रकाशक, गाजियाबाद (उ.प्र.)। मूल्य : रु.350/-। संस्करण : 2011।
- ई-2149, राजाजीपुरम्, लखनऊ-226017 (उ.प्र.)